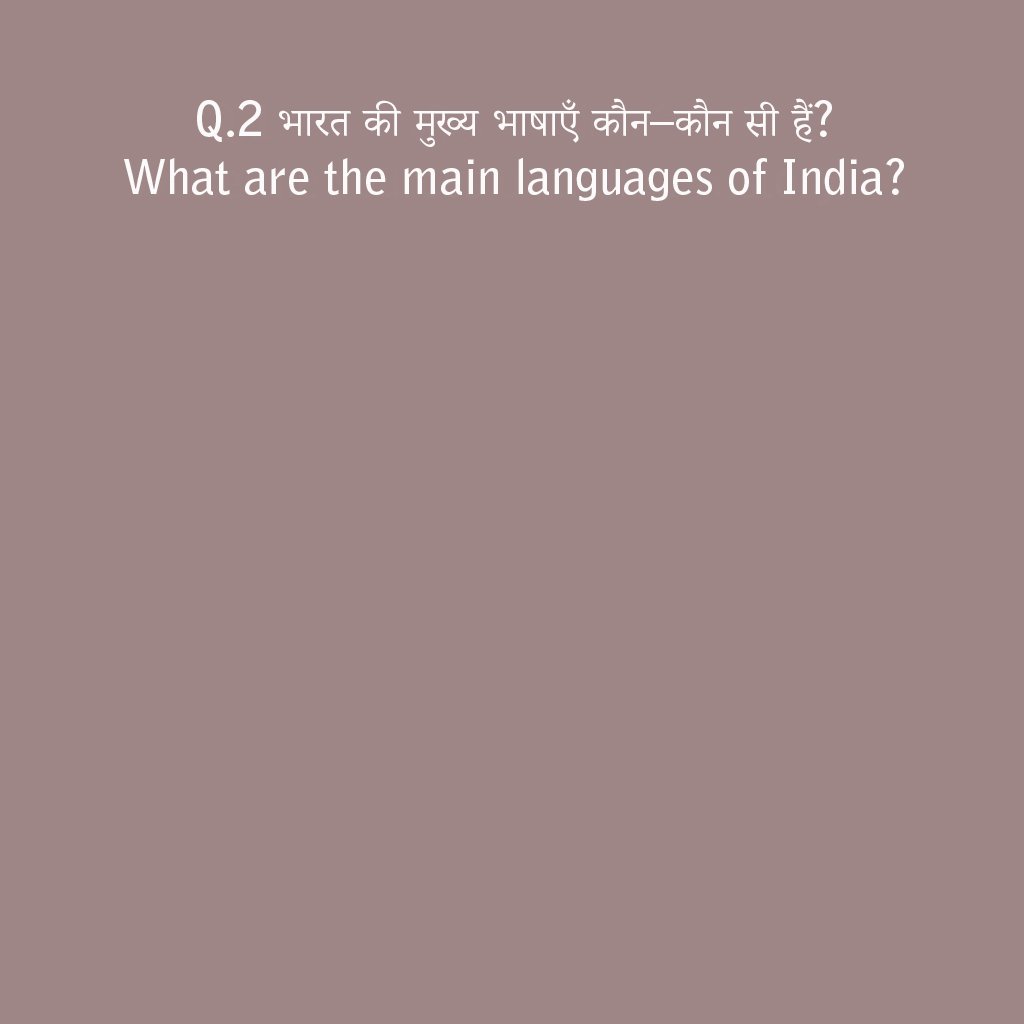भारत की मुख्य भाषाएँ Main languages of India
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
परिचय
भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, जातियाँ, संस्कृतियाँ और भाषाएँ एक साथ पनपती रही हैं। भारतीय समाज की बहुभाषी प्रकृति इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। भारत में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से कई भाषाएँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं। भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि यह संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की वाहक भी होती है।
भारत की भाषाएँ उसकी सांस्कृतिक विविधता का दर्पण हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और बोली है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या इतनी अधिक है कि इसे “भाषाओं का महासागर” कहा जाता है।
भारतीय भाषाओं की विशेषताएँ
- बहुलता और विविधता:
भारत में 122 प्रमुख भाषाएँ और लगभग 1599 बोलियाँ प्रचलित हैं। - भाषाई परिवार:
भारत की भाषाएँ मुख्यतः चार भाषायी परिवारों से संबंधित हैं—- भारोपीय (Indo-Aryan)
- द्रविड़ (Dravidian)
- ऑस्ट्रो-एशियाटिक (Austro-Asiatic)
- चीनी-तिब्बती (Sino-Tibetan)
- संविधान में मान्यता:
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। - भाषाई राज्यों का गठन:
भारत में राज्यों का गठन भी भाषा के आधार पर किया गया है। उदाहरण—आंध्र प्रदेश (तेलुगु), तमिलनाडु (तमिल), महाराष्ट्र (मराठी) आदि।
भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण
1. भारोपीय (Indo-Aryan) भाषाएँ
भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएँ भारोपीय परिवार से संबंधित हैं। देश की लगभग 75% आबादी इन भाषाओं का उपयोग करती है। इन भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है।
मुख्य भारोपीय भाषाएँ
(क) हिंदी
- स्थिति: भारत की राजभाषा।
- लिपि: देवनागरी।
- बोलने वाले: लगभग 60 करोड़ लोग।
- क्षेत्र: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि।
- विशेषता: हिंदी साहित्य में कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा जैसे महान लेखक और कवि हुए हैं। हिंदी सिनेमा ने भी इसे लोकप्रिय बनाया है।
(ख) उर्दू
- लिपि: फारसी-नस्तालिक।
- क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, दिल्ली।
- विशेषता: ग़ज़ल, शायरी और अदब की भाषा। मीर, ग़ालिब, इक़बाल जैसे शायरों की भाषा।
(ग) पंजाबी
- लिपि: गुरुमुखी।
- क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली।
- विशेषता: सिख धर्म के ग्रंथ ‘गुरु ग्रंथ साहिब’ की भाषा।
(घ) बंगाली
- लिपि: बंगला लिपि।
- क्षेत्र: पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम के कुछ भाग।
- विशेषता: रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिमचंद्र, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की भाषा। बंगाली साहित्य ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा पाई।
(ङ) मराठी
- लिपि: देवनागरी।
- क्षेत्र: महाराष्ट्र।
- विशेषता: संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर जैसे संतों की भाषा। मराठी रंगमंच भी प्रसिद्ध है।
(च) गुजराती
- लिपि: गुजराती।
- क्षेत्र: गुजरात।
- विशेषता: महात्मा गांधी और सरदार पटेल की मातृभाषा।
(छ) ओड़िया
- लिपि: ओड़िया लिपि।
- क्षेत्र: ओडिशा।
- विशेषता: ओड़िया साहित्य की समृद्ध परंपरा है।
(ज) असमिया (Assamese)
- लिपि: असमिया लिपि।
- क्षेत्र: असम।
- विशेषता: असम के सांस्कृतिक जीवन की मुख्य भाषा।
(झ) सिंधी
- लिपि: देवनागरी और अरबी।
- क्षेत्र: सिंधी समुदाय में।
(ञ) संस्कृत
- लिपि: देवनागरी।
- विशेषता: भारत की प्राचीनतम और वैज्ञानिक भाषा। वेद, उपनिषद, महाकाव्य संस्कृत में हैं।
2. द्रविड़ (Dravidian) भाषाएँ
द्रविड़ भाषाएँ दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएँ हैं। इनका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्व माना जाता है।
मुख्य द्रविड़ भाषाएँ
(क) तमिल
- लिपि: तमिल लिपि।
- क्षेत्र: तमिलनाडु, श्रीलंका के तमिल बहुल क्षेत्र।
- विशेषता: दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से एक। संगम साहित्य प्रसिद्ध है।
(ख) तेलुगु
- लिपि: तेलुगु लिपि।
- क्षेत्र: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
- विशेषता: इसे “इतालियन ऑफ द ईस्ट” कहा जाता है। काव्यात्मक शैली की भाषा।
(ग) कन्नड़
- लिपि: कन्नड़।
- क्षेत्र: कर्नाटक।
- विशेषता: कन्नड़ साहित्य में पंप, हरिहर, रघवांक जैसे महान कवि।
(घ) मलयालम
- लिपि: मलयालम।
- क्षेत्र: केरल।
- विशेषता: मलयालम फिल्में और साहित्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध।
3. ऑस्ट्रो-एशियाटिक (Austro-Asiatic) भाषाएँ
ये भाषाएँ आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती हैं।
मुख्य भाषाएँ
- संथाली: झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है।
- हो, मुंडारी, खड़िया भी इसी वर्ग में आती हैं।
4. चीनी-तिब्बती (Sino-Tibetan) भाषाएँ
ये भाषाएँ पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित हैं।
मुख्य भाषाएँ
- भूटिया
- मिजो
- नागा भाषाएँ
- मोनपा, लद्दाखी आदि
भारत की 22 संविधानिक भाषाएँ (आठवीं अनुसूची)
| क्रम | भाषा | वर्ग |
|---|---|---|
| 1 | हिंदी | भारोपीय |
| 2 | संस्कृत | भारोपीय |
| 3 | उर्दू | भारोपीय |
| 4 | पंजाबी | भारोपीय |
| 5 | बंगाली | भारोपीय |
| 6 | असमिया | भारोपीय |
| 7 | ओड़िया | भारोपीय |
| 8 | गुजराती | भारोपीय |
| 9 | मराठी | भारोपीय |
| 10 | कश्मीरी | भारोपीय |
| 11 | कोंकणी | भारोपीय |
| 12 | डोगरी | भारोपीय |
| 13 | सिंधी | भारोपीय |
| 14 | तमिल | द्रविड़ |
| 15 | तेलुगु | द्रविड़ |
| 16 | कन्नड़ | द्रविड़ |
| 17 | मलयालम | द्रविड़ |
| 18 | संथाली | ऑस्ट्रो-एशियाटिक |
| 19 | बोडो | चीनी-तिब्बती |
| 20 | मैथिली | भारोपीय |
| 21 | मणिपुरी (मैतेई) | चीनी-तिब्बती |
| 22 | नेपाली | भारोपीय |
विदेशी प्रभाव वाली भाषाएँ
भारत में अंग्रेजी भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। यह न्यायपालिका, उच्च शिक्षा और वैश्विक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भाषाई विविधता का महत्व
- सांस्कृतिक धरोहर:
प्रत्येक भाषा अपने साथ एक अनूठी संस्कृति लेकर चलती है। - सामाजिक पहचान:
भाषा से व्यक्ति की सामाजिक और भौगोलिक पहचान जुड़ी होती है। - आर्थिक विकास:
भाषा के आधार पर क्षेत्रीय साहित्य, सिनेमा, संगीत, और मीडिया का विकास होता है। - राष्ट्रीय एकता में सहयोग:
विविधता के बावजूद भारत की भाषाएँ एकता का सूत्र बनाती हैं।
भाषा से जुड़ी चुनौतियाँ
- भाषाई विवाद:
हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच कई बार विवाद हुआ है। - बोलियों का लुप्त होना:
आधुनिक समय में कई स्थानीय बोलियाँ विलुप्त हो रही हैं। - भाषाई असंतुलन:
कुछ भाषाओं को ज्यादा प्राथमिकता मिलने से अन्य भाषाओं को खतरा है।
निष्कर्ष
भारत की भाषाएँ उसकी आत्मा हैं। यह विविधता भारत की शक्ति है, न कि कमजोरी। प्रत्येक भाषा का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि हर भाषा अपने आप में एक संस्कृति, इतिहास और परंपरा की प्रतिनिधि है।
आज आवश्यकता है कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करें और बहुभाषिक भारत की गरिमा को बनाए रखें।
“भारत की भाषाएँ, भारत की पहचान हैं। इनका संरक्षण ही हमारी असली संस्कृति की रक्षा है।”