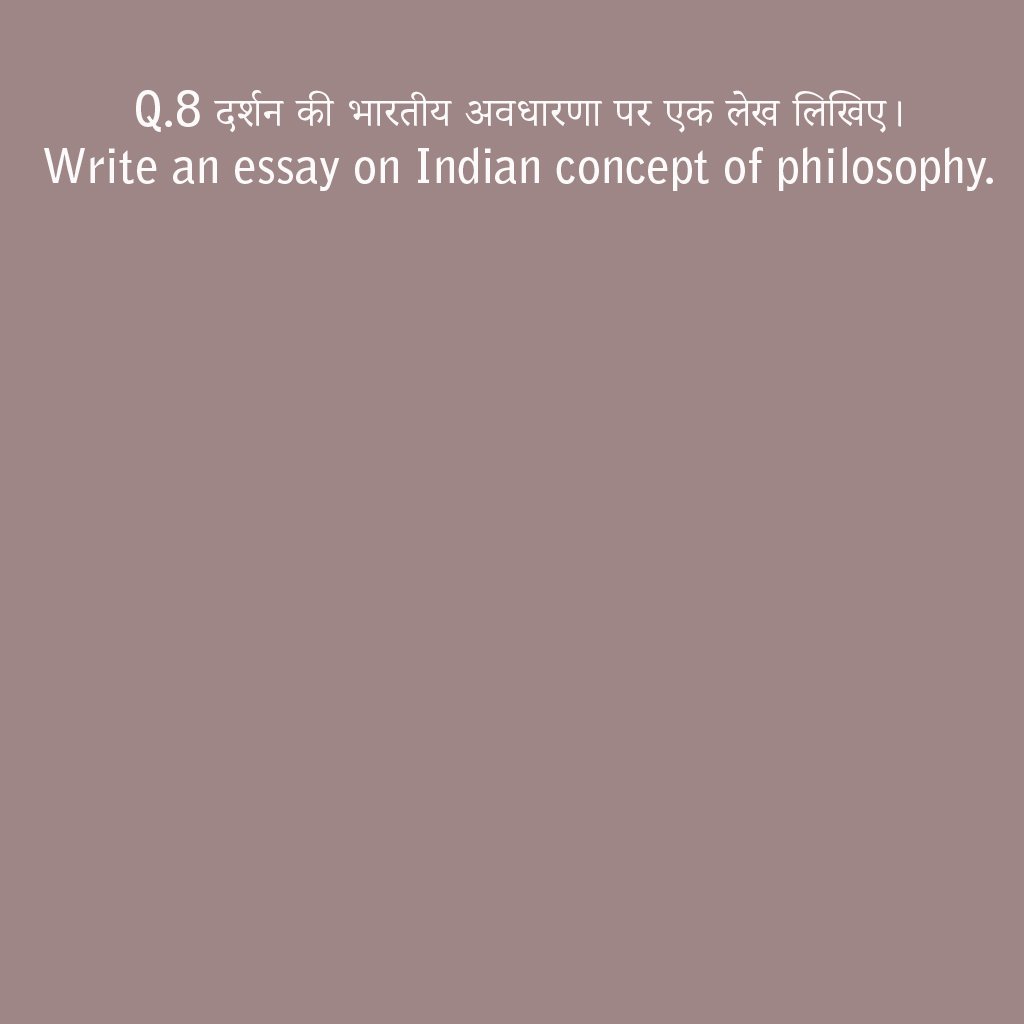दर्शन की भारतीय अवधारणा Indian concept of philosophy
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
परिचय
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार दर्शन है।
‘दर्शन’ का सामान्य अर्थ देखने से है, लेकिन भारतीय संदर्भ में दर्शन का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं को देखना नहीं, बल्कि सत्य को समझना, आत्मा की खोज करना और जीवन के रहस्यों को जानना है।
भारतीय दर्शन ने केवल भौतिक दुनिया की नहीं बल्कि आत्मा, परमात्मा, जीवन-मरण, पुनर्जन्म, मोक्ष, धर्म, नीति, कर्म और ब्रह्मांड के रहस्यों पर गहन विचार किया है।
भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष, यानी जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और यही ज्ञान दर्शन के माध्यम से प्राप्त होता है।
दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ
व्युत्पत्ति
संस्कृत में ‘दर्शन’ शब्द की उत्पत्ति ‘दृश’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है— देखना, जानना, अनुभव करना।
दर्शन का शाब्दिक अर्थ है—
- सत्य का साक्षात्कार करना
- वास्तविकता को जानना
- तत्त्वों के स्वरूप को समझना
दर्शन का उद्देश्य
भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है—
- जीवन के परम सत्य की खोज
- जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना
- आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना
- मोक्ष की प्राप्ति
भारतीय दर्शन की विशेषताएँ
1. आध्यात्मिक दृष्टिकोण
भारतीय दर्शन मुख्यतः आध्यात्मिक है। इसका लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म की पहचान करना है।
2. जीवन के चार पुरुषार्थों की खोज
भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन के चार उद्देश्य हैं—
- धर्म (कर्तव्य)
- अर्थ (धन)
- काम (इच्छा की पूर्ति)
- मोक्ष (मुक्ति)
दर्शन इन चारों पुरुषार्थों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
3. मोक्ष प्रधानता
भारतीय दर्शन मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह संसार के बंधनों से छुटकारा पाने की विद्या है।
4. तात्त्विक विचार
दर्शन केवल तर्क या बहस नहीं है, बल्कि आत्मा, ब्रह्म, जगत, जीवन-मरण, पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों की खोज है।
भारतीय दर्शन के प्रकार
भारतीय दर्शन को दो भागों में बाँटा जाता है:
1. आस्तिक दर्शन (Theistic Schools)
जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। इन्हें षड्दर्शन कहा जाता है।
| दर्शन | प्रवर्तक |
|---|---|
| सांख्य दर्शन | कपिल मुनि |
| योग दर्शन | पतंजलि |
| न्याय दर्शन | गौतम |
| वैशेषिक दर्शन | कणाद |
| मीमांसा दर्शन | जैमिनि |
| वेदांत दर्शन | बादरायण (व्यास) |
2. नास्तिक दर्शन (Atheistic Schools)
जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते।
| दर्शन | प्रवर्तक |
|---|---|
| जैन दर्शन | महावीर स्वामी |
| बौद्ध दर्शन | गौतम बुद्ध |
| चार्वाक दर्शन | बृहस्पति |
भारतीय दर्शन के षड्दर्शन का परिचय
1. सांख्य दर्शन
- संसार की उत्पत्ति और कारणों पर विचार करता है।
- प्रकृति और पुरुष की द्वैत सिद्धांत को मानता है।
- परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता।
- मोक्ष को अज्ञान का नाश मानता है।
2. योग दर्शन
- पतंजलि द्वारा प्रणीत।
- योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया।
- अष्टांग योग— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
3. न्याय दर्शन
- तर्क और प्रमाण के आधार पर सत्य की खोज।
- महर्षि गौतम ने न्यायसूत्र की रचना की।
- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को प्रमाण मानता है।
4. वैशेषिक दर्शन
- पदार्थों का वर्गीकरण करता है।
- अणुवाद का समर्थन करता है।
- पदार्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और संबंध का विश्लेषण।
5. मीमांसा दर्शन
- वेदों के कर्मकांड पर आधारित।
- यज्ञ और वैदिक कर्मों के महत्व पर बल।
- आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म को मान्यता।
6. वेदांत दर्शन
- ब्रह्म और आत्मा की अद्वैतता।
- ब्रह्म ही जगत का कारण है।
- आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को लोकप्रिय बनाया।
नास्तिक दर्शन का परिचय
1. जैन दर्शन
- अहिंसा पर मुख्य बल।
- आत्मा और कर्म का सिद्धांत।
- तीर्थंकरों की परंपरा।
- मोक्ष के लिए तप और संयम आवश्यक।
2. बौद्ध दर्शन
- चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग।
- अनित्य, अनात्मा और दुख की अवधारणा।
- निर्वाण को अंतिम लक्ष्य।
3. चार्वाक दर्शन
- भौतिकवाद को मान्यता।
- इंद्रिय सुख को जीवन का उद्देश्य मानता है।
- न आत्मा, न पुनर्जन्म, न परलोक।
भारतीय दर्शन की मुख्य अवधारणाएँ
1. आत्मा (Self)
- भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर, अजर और अविनाशी माना गया है।
- आत्मा शरीर का नहीं, बल्कि चेतना का मूल स्रोत है।
2. ब्रह्म (Ultimate Reality)
- ब्रह्म ही जगत का कारण और आधार है।
- अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना गया है।
3. कर्म (Action)
- प्रत्येक क्रिया का फल निश्चित है।
- अच्छे कर्म से सुख और बुरे कर्म से दुःख।
4. पुनर्जन्म (Rebirth)
- आत्मा मृत्यु के बाद नया शरीर धारण करती है।
- कर्म के अनुसार जन्म मिलता है।
5. मोक्ष (Liberation)
- जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति।
- मोक्ष को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है।
भारतीय दर्शन की विशेषताएँ
1. जीवन और जगत के रहस्यों की खोज
- भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है।
- जीवन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है।
2. भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन
- अर्थ और काम की प्राप्ति के साथ धर्म और मोक्ष की साधना।
3. अनुभव और साक्षात्कार पर बल
- केवल पुस्तक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मानुभूति महत्वपूर्ण है।
4. सहिष्णुता और विविधता
- विभिन्न मतों का सम्मान।
- किसी एक सत्य पर जोर नहीं, बल्कि सत्य की विविध व्याख्याएँ।
भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का अंतर
| भारतीय दर्शन | पश्चिमी दर्शन |
|---|---|
| आध्यात्मिक | भौतिक और मानसिक |
| मोक्ष पर बल | तर्क और विश्लेषण पर बल |
| आत्मा और ब्रह्म की खोज | मानव समाज की समस्याओं पर विचार |
| जीवन पद्धति से जुड़ा | बौद्धिक विश्लेषण |
भारतीय दर्शन की प्रासंगिकता
1. आधुनिक जीवन में समाधान
- तनाव, अवसाद और चिंता से मुक्ति के उपाय।
- योग और ध्यान का महत्व।
2. नैतिक और सामाजिक संतुलन
- कर्म, धर्म और मोक्ष का संतुलन।
- समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना।
3. वैश्विक मानवता के लिए संदेश
- “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना।
- सबका कल्याण ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य।
निष्कर्ष
भारतीय दर्शन केवल पुस्तकालयों में बंद विचारधारा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है।
यह आत्मा और ब्रह्म की खोज का मार्ग है।
यह दर्शन व्यक्ति, समाज और विश्व के कल्याण की भावना से प्रेरित है।
भारतीय मनीषियों ने दर्शन को जीवन का आधार बनाया और कहा—
“तत्त्वमसि” (तू वही है)
“अहं ब्रह्मास्मि” (मैं ब्रह्म हूँ)
आज के समय में जब मानव भौतिकता के जाल में उलझा है, भारतीय दर्शन ही उसे सही मार्ग दिखा सकता है।
यह दर्शन केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है।