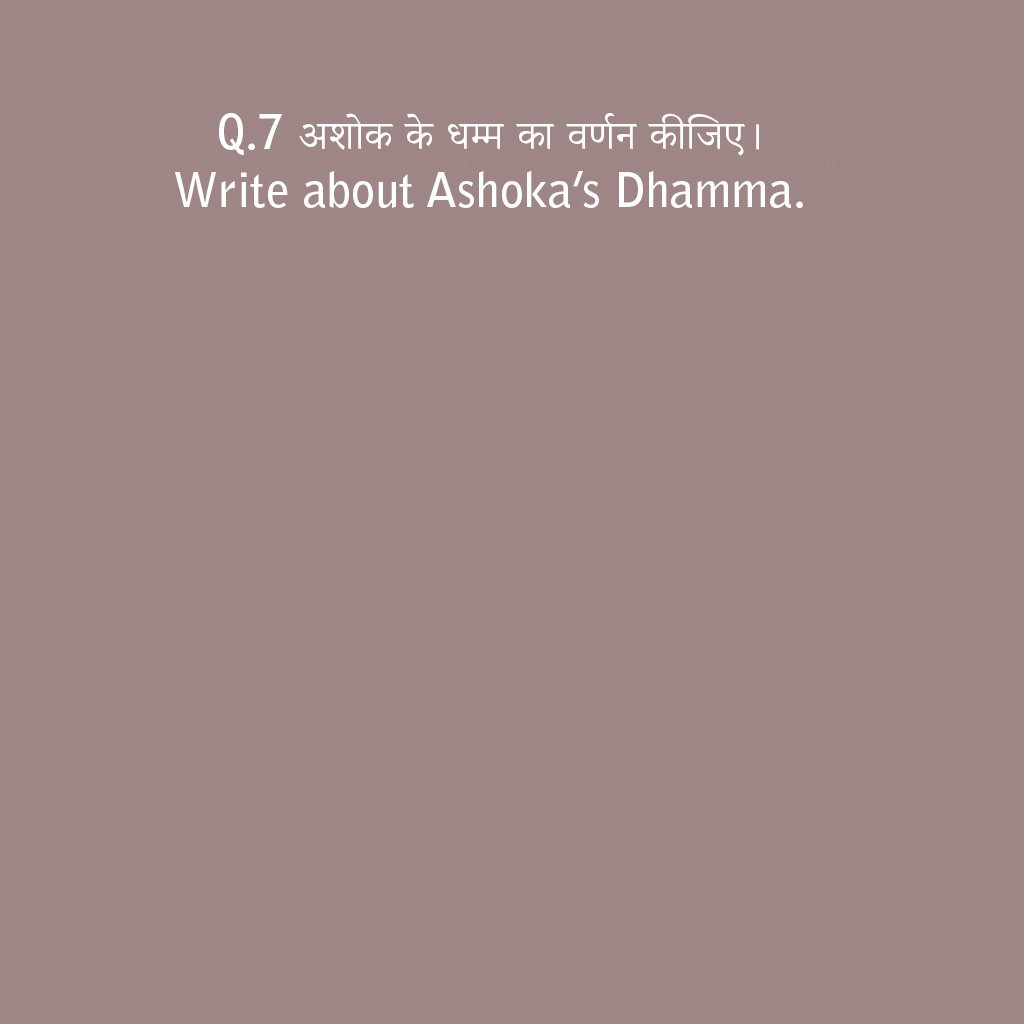अशोक के धम्म का वर्णन Description of Ashoka’s Dhamma
शुरुआत से अंत तक जरूर पढ़ें।
1. प्रस्तावना: मौर्य सम्राट अशोक और धम्म
मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक (273–232 ई.पू.) भारतीय इतिहास में उस शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता, धर्म और मानवीय मूल्यों से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास किया। कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) में हुए भीषण रक्तपात के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया और शासन को धम्म (Dhamma) की भावना पर आधारित किया।
अशोक का धम्म किसी विशेष धर्म का उपदेश नहीं था, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक संहिता था, जिसका उद्देश्य समाज में सद्भाव, अहिंसा, सत्य, करुणा, भाईचारा और धर्म सहिष्णुता स्थापित करना था।
2. धम्म की परिभाषा
‘धम्म’ शब्द पाली भाषा के ‘धर्म’ का रूप है। अशोक के धम्म का अर्थ है—
- नैतिक मूल्यों और सदाचारों का समुच्चय।
- ऐसा आचार-संहिता जो न केवल मनुष्य को, बल्कि समाज, प्रशासन और राज्य को भी मानवता, न्याय और दया के सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित करे।
अशोक के धम्म का उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान और सामाजिक कल्याण था।
3. धम्म के उद्भव की पृष्ठभूमि
3.1 कलिंग युद्ध का प्रभाव
- 261 ई.पू. में कलिंग युद्ध में लगभग एक लाख लोग मारे गए और डेढ़ लाख लोग कैद किए गए।
- अशोक के शिलालेखों (विशेषकर तेरहवाँ शिलालेख) में वह इस युद्ध की विभीषिका का वर्णन करते हैं।
- युद्ध की इस भयावहता से प्रभावित होकर उन्होंने हिंसा छोड़ने और धर्म मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
3.2 बौद्ध धर्म का प्रभाव
- कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आए।
- बौद्ध सिद्धांत—अहिंसा, करुणा, दया और मध्यम मार्ग—ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।
- हालांकि अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, उसमें सभी धर्मों और नैतिक विचारों का सार था।
3.3 बहु-धार्मिक समाज की आवश्यकता
- मौर्य साम्राज्य विशाल और बहुजातीय था। इसमें बौद्ध, जैन, वैदिक, आजीवक और अन्य संप्रदाय साथ रहते थे।
- अशोक का धम्म सभी धर्मों को सम्मान और सहिष्णुता देने की नीति थी, जिससे समाज में सद्भावना बनी रहे।
4. अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत
अशोक के शिलालेखों और अभिलेखों से उसके धम्म के मुख्य तत्वों को इस प्रकार समझा जा सकता है:
4.1 अहिंसा
- अशोक ने अहिंसा को सर्वोपरि माना।
- उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और शिकार को सीमित किया।
- उनका मानना था कि हिंसा केवल विनाश लाती है; सभी प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए।
4.2 सत्य और ईमानदारी
- धम्म में सत्य बोलना, ईमानदारी और न्याय पर जोर दिया गया।
- प्रशासनिक कार्यों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया गया।
4.3 सहिष्णुता और धर्म सम्मान
- अशोक का मानना था कि सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए।
- बारहवाँ शिलालेख में वे कहते हैं—“जो व्यक्ति अपने धर्म का आदर करता है, उसे दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए।”
4.4 करुणा और दया
- उन्होंने दीन-दुखियों, वृद्धों, कैदियों और बीमारों के प्रति करुणा की नीति अपनाई।
- जेलों में दंड नीति को नरम किया गया।
4.5 पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता
- धम्म में माता-पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, छोटे भाई-बहनों से प्रेम और परिवार में शांति को महत्व दिया गया।
- उन्होंने पारिवारिक कर्तव्यों को धार्मिक कर्तव्य के समान माना।
4.6 प्राणी संरक्षण
- पशु-पक्षियों की हत्या और बलि पर रोक लगाई।
- राजकीय अश्वमेध जैसे वैदिक बलि यज्ञों को त्याग दिया।
- कई अभिलेखों में उन्होंने बताया कि वे हर जीव में आत्मा का सम्मान करते हैं।
5. धम्म के प्रसार के उपाय
अशोक ने अपने धम्म को समाज में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए।
5.1 शिलालेख और स्तंभलेख
- उन्होंने शिलालेखों और स्तंभों पर धम्म के संदेश खुदवाए।
- ये लेख पूरे मौर्य साम्राज्य में—कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक—स्थापित किए गए।
5.2 धम्म महामात्रों की नियुक्ति
- अशोक ने विशेष अधिकारियों ‘धम्म महामात्र’ को नियुक्त किया, जो धम्म की शिक्षा, जनकल्याण और नैतिक संदेश फैलाने का काम करते थे।
5.3 बौद्ध धर्म प्रचार और यात्राएँ
- अशोक ने स्वयं धर्म यात्राएँ कीं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में दूत भेजे।
- उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा, जहाँ बौद्ध धर्म स्थापित हुआ।
5.4 चिकित्सा और कल्याणकारी कार्य
- उन्होंने मानव और पशुओं के लिए चिकित्सालयों की स्थापना की।
- पेड़-पौधों का रोपण, कुएँ और सराय बनवाए ताकि जनता को सुविधा हो।
6. अशोक के धम्म की प्रशासनिक भूमिका
अशोक का धम्म सिर्फ व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासन का भी आधार था।
- प्रशासन में दया और न्याय का समावेश।
- कठोर कर-वसूली के स्थान पर जन-हितकारी नीति।
- अहिंसा और दंड की नरमी को सरकारी नीति में शामिल किया गया।
- राजा को “धम्म का पिता” माना गया जो प्रजा के कल्याण के लिए उत्तरदायी है।
7. धम्म और समाज सुधार
अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था:
- सामाजिक समरसता और धर्म-सहिष्णुता।
- जाति-पाति और धार्मिक द्वेष को समाप्त करना।
- नैतिकता, करुणा और जनकल्याण को राज्य की नींव बनाना।
इससे समाज में शांति और स्थिरता आई।
8. अशोक के धम्म की विशेषताएँ
- यह किसी विशेष धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक संहिता था।
- अहिंसा और करुणा इसका मूल आधार था।
- इसमें सभी धर्मों के प्रति समान आदर की बात थी।
- इसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक नैतिकता का संतुलित मेल था।
- यह राज्य और प्रशासन की नीतियों का भी मार्गदर्शन करता था।
9. अशोक के धम्म का महत्व
- अशोक का धम्म भारतीय इतिहास में एक अनोखा प्रयोग था जहाँ राजनीतिक सत्ता को नैतिक मूल्यों से जोड़ा गया।
- इसके कारण अशोक को ‘धम्माशोक’ और ‘प्रजापिता’ कहा गया।
- धम्म का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और एशिया के अन्य देशों में भी देखा गया।
- यह आज भी मानवता, सहिष्णुता और शांति का संदेश देता है।
10. धम्म की सीमाएँ
- धम्म अत्यधिक नैतिकता-प्रधान होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से कठोर शासकीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता था।
- उत्तराधिकारियों की कमजोरी और धम्म-नीति की वजह से मौर्य साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर हुआ।
- इसकी अत्यधिक अहिंसा-नीति ने सेन्य-तंत्र को शिथिल बना दिया।
11. निष्कर्ष
अशोक का धम्म एक ऐसा मानव-केन्द्रित शासन दर्शन था, जिसने भारतीय राजनीति और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो धम्म नीति अपनाई, उसने साम्राज्य में शांति, धर्म सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया।
यद्यपि धम्म का राजनीतिक दृष्टि से कुछ कमजोर पहलू रहे, लेकिन इसकी नैतिक और मानवीय शक्ति के कारण अशोक विश्व इतिहास में ‘धम्म सम्राट’ के रूप में अमर हो गए।