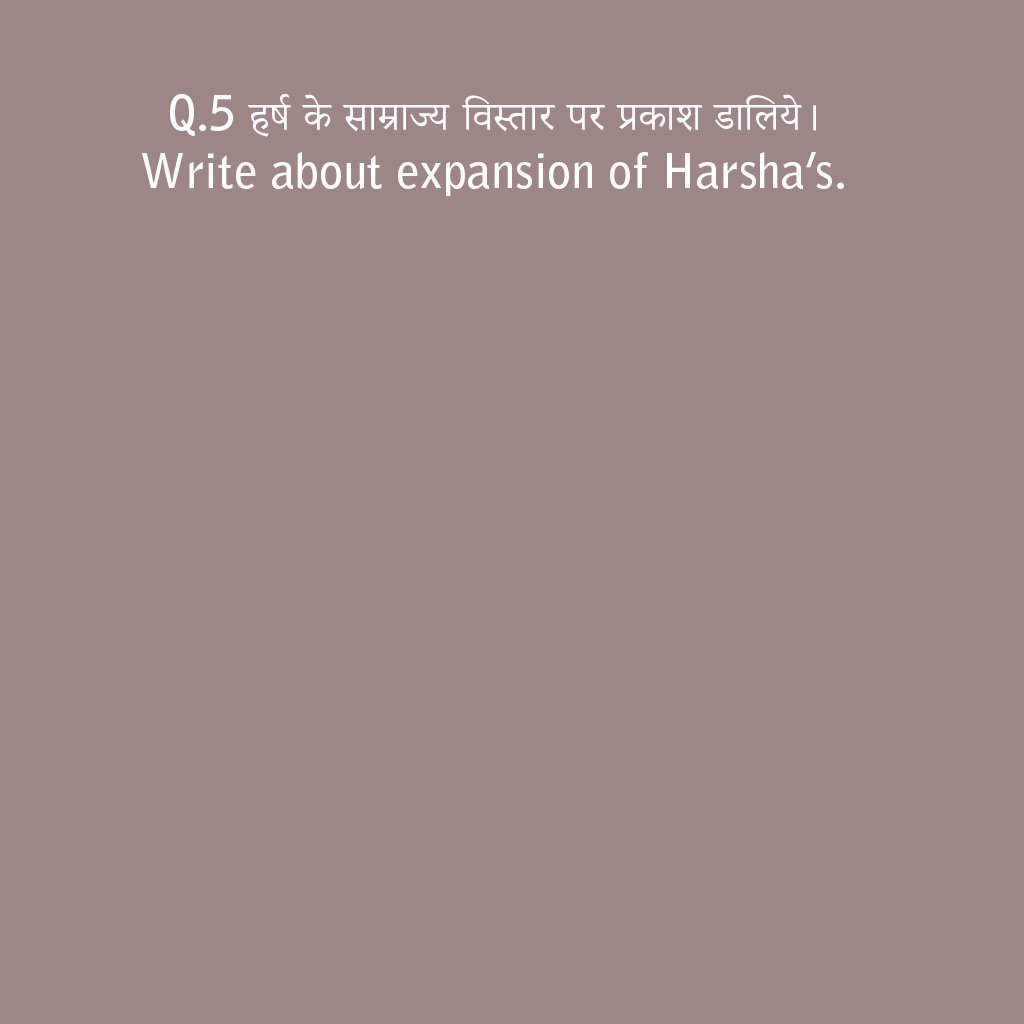हर्ष के साम्राज्य‑विस्तार पर प्रकाश Light on the expansion of Harsha’s empire
शुरुआत से अंत तक जरूर पढ़ें।
1. प्रस्तावना: “उत्तर भारत का सम्राट” बनने की यात्रा
हर्षवर्धन (≈ 606–647 ई.) गुप्तोत्तर युग के उस शासक का नाम है जिसने लगभग समूचे उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक इकाई के रूप में जोड़ा। उनके शासनकाल में कनौज (कन्नौज) नयी साम्राज्य-राजधानी के रूप में उभरा, और हर्ष ने एक ओर सैन्य अभियानों द्वारा, तो दूसरी ओर कूटनीति, वैवाहिक-संबंधों और सामन्तीय (feudatory) व्यवस्था के सहारे अपना प्रभाव-क्षेत्र बहुत दूर तक फैला दिया। तथापि, दक्षिण में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा पर उनकी दक्षिणगामी महत्वाकांक्षा रोक दी—और यही उनकी विस्तार-नीति की अंतिम वास्तविक सीमा सिद्ध हुई। हर्ष के साम्राज्य-विस्तार को समझने के लिए पहले उनके वंश, प्रारम्भिक राजनीतिक परिदृश्य और शक्ति-संघर्षों को देखना होगा।
2. वंश, पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारम्भिक राजनीतिक परिदृश्य
- हर्ष पुष्यभूति/वर्धन वंश के शासक थे। उनके पिता प्रभाकरवर्धन थानेसर (आधुनिक हरियाणा के निकट) के राजा थे।
- बड़े भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्रृी (राज्यश्री)—जो मौखरी शासक ग्रहारवर्मन से विवाहित थीं—हर्ष के जीवन और प्रारम्भिक राजनीति के केंद्रीय पात्र हैं।
- कनौज के मौखरी और थानेसर के वर्धन—इन दोनों घरानों का मैत्री-संबंध (राज्यश्रृी के विवाह के द्वारा) पहले से ही था। इससे उत्तर भारत के राजनीतिक गठबंधनों में वर्धन-मौखरी ब्लॉक एक सशक्त धुरी बन गया था।
- इस समय बंगाल/गौड़ के शशांक, वल्लभियों (वालभी/वल्लभी), मालवा के परमार/आलोपिक शक्तियाँ, और दक्षिण के चालुक्य—ये सब अलग-अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं, जिनसे हर्ष को समीकरण बनाना या भिड़ना था।
3. संकट और अवसर: राज्यवर्धन की मृत्यु, राज्यश्री का अपमान और हर्ष का सिंहासनारोहन
- मौखरी राजा ग्रहारवर्मन को गौड़ के शशांक ने आक्रमण कर मार दिया। इससे राज्यश्री विधवा हुईं।
- राज्यवर्धन (हर्ष के बड़े भाई) ने बहन और मौखरी-संबंधी राज्य का प्रतिशोध लेने के लिए सैन्य अभियान चलाया, पर वे भी षड्यंत्र/धोखे से (अनेक स्रोतों के मतान्तर हैं, परंपरा में प्रायः शशांक का नाम आता है) मारे गए।
- परिवार पर आये इस गहरे संकट ने युवक हर्ष (लगभग 16 वर्ष) को 606 ई. के आस-पास राजसिंहासन संभालने पर मजबूर किया।
- हर्ष ने सबसे पहले राज्यश्री का उद्धार किया (कथा है कि वह दुःखवश वन में चली गई थीं) और फिर अपने मौखरी-संबंधियों के हितों की रक्षा की ठानी। यही से उनका कनौज-केन्द्रित “उत्तर भारतीय साम्राज्य” बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होता है।
4. कनौज को राजधानी बनाना: प्रतीक और राजनीति
- हर्ष ने शीघ्र ही समझ लिया कि कनौज (कन्नौज), जो पहले से ही गंगा-यमुना दोआब के हृदय-क्षेत्र में एक सामरिक-आर्थिक केंद्र था, साम्राज्य के लिए अधिक उपयुक्त राजधानी है।
- कनौज को अपना मुख्यालय बनाकर हर्ष ने मौखरी राज्य की विरासत भी सम्हाली और गंगा के मैदानी इलाक़े पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाए।
- राजनीतिक संदेश साफ़ था: “थानेसर के क्षेत्रीय राजा” से “कनौज के साम्राज्याधिपति” तक—हर्ष ने शक्ति का भौगोलिक और वैधानिक पैमाना बदल दिया।
5. पश्चिम, पूर्व और उत्तर में विस्तार: प्रत्यक्ष विजय, कर-सुजेरैनिटी और सामन्तीय नेटवर्क
हर्ष की विस्तार-रणनीति को तीन स्तरों पर समझ सकते हैं:
- प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहित क्षेत्र (जहाँ उनका सीधा प्रशासन था)।
- सामन्त/उप-राज्य (जो कर/उपहार देते थे, और हर्ष की अधिराज्यता स्वीकारते थे)।
- मैत्री-संधि वाले राज्य (जहाँ वैवाहिक/कूटनीतिक रिश्ता था, जैसे वल्लभी)।
5.1 पूर्व की ओर: शशांक और मगध/गौड़ पर प्रभाव
- हर्ष की शुरुआती चुनौती गौड़ (बंगाल) के शशांक थे।
- आरम्भ में शशांक के कारण ही वर्धन-मौखरी घराने पर संकट आया; हर्ष ने प्रति-आक्रमण के प्रयास किए।
- समय के साथ, शशांक की मृत्यु के बाद, हर्ष ने मगध और मध्य गंगा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और कनौज से बिहार तक मजबूत पकड़ बना ली।
- बंगाल/गौड़ पर उनका सीधा-स्थायी नियंत्रण इतिहासकारों के बीच विवादित है; पर इतना निश्चित है कि पूर्वी भारत में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया और काशी, पाटलिपुत्र, वैशाली, नालंदा जैसे केंद्र उनकी छत्र-छाया में आए।
5.2 पश्चिम और उत्तर-पश्चिम: कश्मीर, सिंध, पंजाब
- पंजाब, थानेसर, कश्मीर तक हर्ष का प्रभाव फैला। कई क्षेत्रों ने उन्हें सामन्त/करदाता शासक के रूप में स्वीकार किया।
- कश्मीर के बारे में ह्वेनसांग (ह्यूएन त्सांग/युआनच्वांग) के वृत्तांत सहित कई स्रोत हर्ष की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हैं, पर यह कई बार औपचारिक अधिराज्यता (suzerainty) के रूप में रहा—अर्थात वहाँ के स्थानीय शासक बने रहे, पर हर्ष का सर्वोच्च अधिकार मानते थे।
- सिंध और राजस्थान के कुछ भाग तक भी उनका प्रभावकारी प्रभुत्व माना जाता है, जहाँ से उपहार/कर आता था और हर्ष के आदेश/अभियोग स्वीकारे जाते थे।
5.3 मध्य भारत: मालवा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, विदिशा
- मालवा (आवंती) और आस-पास के क्षेत्रों में भी हर्ष की विजय-गाथाएँ मिलती हैं।
- ये क्षेत्र उत्तर और दक्कन के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गलियारा थे; यहाँ प्रभुत्व बनाये रखने से दक्कन में प्रवेश (या उसकी रोकथाम) के अवसर नियंत्रित रहते थे।
- कई छोटे-छोटे राजाओं को हर्ष ने सामन्त के रूप में अपने अधीन रखा। उनके दार्शनिक-महादान (प्रयाग) में इनकी उपस्थितियाँ और उपहार इसका संकेत देती हैं।
5.4 वल्लभी (गुजरात) से संबंध: युद्ध से संधि तक
- गुजरात/वल्लभी के साथ प्रारम्भ में संघर्ष हुआ, पर बाद में कूटनीतिक सन्धि और वैवाहिक रिश्ते बने (कई स्रोत बताते हैं कि हर्ष ने अपनी एक राजकुमारी का विवाह वल्लभी नरेश से करवाया)।
- इसके बाद वल्लभी हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण/मित्र-सामन्त स्थिति में आ गया, जिससे पश्चिमी तट पर भी हर्ष का प्रभाव-संतुलन बना रहा।
6. दक्षिण की दिशा: नर्मदा पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोका गया विस्तार
- हर्ष का दक्षिण में सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी था चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय (पुलकेशी II), जिसकी राजधानी बादामी (कर्नाटक) में थी।
- हर्ष ने दक्कन में प्रवेश कर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की, पर नर्मदा नदी के पुश्ते पर पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित/रोका।
- इस संघर्ष की तिथि के बारे में मतभेद हैं—कई इतिहासकार इसे लगभग 618–619 ई. के आसपास मानते हैं, जबकि ऐहोल (Aihole) अभिलेख (634–35 ई.) का संदर्भ लेते हुए कुछ इसे 630 के दशक से भी जोड़ते हैं। निष्कर्ष यह कि नर्मदा हर्ष की दक्षिणी सीमा बन गयी।
- इस हार का प्रभाव यह हुआ कि हर्ष ने दक्षिण की महत्वाकांक्षा त्याग कर उत्तर भारत का एकीकृत सम्राज्य और पूर्व-पश्चिम की कूटनीतिक संतुलन-नीति को प्राथमिकता दी।
7. साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा: प्रत्यक्ष शासन बनाम सामन्तीय ढाँचा
- हर्ष का साम्राज्य एक “सघन केंद्रीकृत राज्य” की तुलना में “विस्तृत अधिराज्य” (empire of suzerainty) के रूप में सही समझा जाता है।
- गंगा-यमुना दोआब, मगध, पूर्वी यूपी-बिहार, पंजाब का बड़ा भाग—इन पर हर्ष का प्रत्यक्ष शासन था।
- कश्मीर, नेपाल, सिंध, राजस्थान, वल्लभी, उड़ीसा के कुछ भाग आदि में उनका शासन औपचारिक अधिराज्य (overlordship) की तरह था—अर्थात स्थानीय राजा/सामन्त अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाते थे, पर हर्ष के नाम का सिक्का, कर-प्रेषण, और राज-स्वीकार्यता बनी रहती थी।
- प्रशासनिक स्तर पर जिलों/प्रदेशों (भुक्ति), फिर विषय, विल (कस्बे/गाँवों के समूह), और गाँव तक अधिकारी-पद्धति चलती थी—यह गुप्तकालीन संरचनाओं से बहुत अलग नहीं थी, पर हर्ष ने इसे सक्रिय सैन्य-सामन्तीय ढाँचे से जोड़कर राज्य-विस्तार का उपकरण बनाया।
8. धर्म, दान और राजनीति: प्रयाग के महादान और अधिराज्य का वैधीकरण
- हर्ष ने प्रयाग (आधुनिक प्रयागराज/इलाहाबाद) में हर पाँच वर्ष में एक महाधर्म-महादान (महामोक्ष परिषद / क्विन्केनियल असेंबली) आयोजित की—जहाँ विशाल दान, बहसें, और धार्मिक-वैचारिक संवाद होते थे।
- यह आयोजन केवल धर्म-निष्ठा का प्रतीक नहीं था, बल्कि राजकीय वैधीकरण (legitimacy) का भी माध्यम था—दूर-दूर के सामन्त/राज्य यहाँ उपस्थित होकर हर्ष की सर्वोच्चता का औपचारिक स्वीकार करते थे।
- ह्वेनसांग (ह्यूएन त्सांग/युआनच्वांग) के वृत्तांत इन सम्मेलनों, दानों, और हर्ष की प्रतिष्ठा का जीवंत चित्र देते हैं।
- कन्नौज (643 ई.) का बौद्ध धर्म-सम्मेलन और नालंदा का संरक्षण—ये सब हर्ष के धार्मिक सहिष्णु, पर साथ ही राज्य-वैधता को पुष्ट करने वाले कदम थे।
9. हर्ष के साम्राज्य की अनुमानित भौगोलिक सीमा
(इतिहासकारों में सूक्ष्म मतभेद हैं; यहाँ एक समावेशी, किन्तु विवेकपूर्ण रेखांकन दिया जा रहा है)
- उत्तर-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक: पंजाब, थानेसर, कन्नौज, मगध, वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मिथिला, कश्मीर (सामन्तीय स्वीकृति), नेपाल (सामन्तीय), और बंगाल/गौड़ के महत्त्वपूर्ण हिस्सों पर प्रभाव (शशांक के पश्चात)।
- पश्चिम की ओर: राजस्थान के बड़े हिस्से, मालवा, और वल्लभी/गुजरात के साथ मैत्री-संबंध (जो प्रभाव-क्षेत्र में गिने जा सकते हैं)।
- दक्षिण की ओर: नर्मदा तक का भाग; इसके बाद चालुक्य प्रभुत्व।
- पूर्व-दक्षिण (ओडिशा/कलिंग): कुछ हिस्सों में प्रभाव, पर वहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष शासन का दावा कठिन है; कई स्थानीय-क्षेत्रीय शक्तियाँ विद्यमान थीं।
संक्षेप में कहा जाए तो हर्ष का प्रत्यक्ष/मजबूत शासन उत्तर भारत के “गंगा के मैदान” में था, जबकि कश्मीर, नेपाल, सिंध, राजस्थान, वल्लभी, उड़ीसा आदि में उनकी अधिराज्यता/सामन्तीय नेटवर्क के रूप में प्रभाव देखा जाता है; दक्कन और दक्षिण भारत उनके अधिकार से बाहर रहा।
10. स्रोत: हरषचरित, ह्वेनसांग और अभिलेख
हर्ष के साम्राज्य-विस्तार को समझने में मुख्य स्रोत हैं:
- बाणभट्ट की ‘हर्षचरित’: दरबारी रचना है, अतः राज-गौरव का पक्षपात सम्भव; फिर भी राजनीतिक घटनाओं, राजवंशीय वृत्तांत और हर्ष की छवि को समझने का यह अनमोल स्रोत है।
- ह्वेनसांग (युआनच्वांग) का यात्रा-वृत्तांत: 7वीं सदी के इस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के दरबार और भारत के अनेक क्षेत्रों का प्रत्यक्ष वर्णन किया। यह अपेक्षाकृत तटस्थ एवं विवरणपूर्ण स्रोत माना जाता है।
- ऐहोल अभिलेख (634–35 ई.): चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, जो हर्ष-पुलकेशिन संघर्ष का संकेत देता है और हर्ष के दक्षिणी विस्तार की विफलता को समकालीन दृष्टि से प्रमाणित करता है।
- अन्य शिलालेख, मुद्राएँ और परवर्ती इतिहासकारों की व्याख्याएँ—जो व्यापक चित्र बनाने में सहायक हैं, पर जिनमें मतभेद भी पाए जाते हैं।
11. विस्तार-नीति की सीमाएँ और चुनौतियाँ
- दक्षिण का अभेद्य किला: चालुक्य साम्राज्य की शक्ति, भौगोलिक दूरी, और नर्मदा के पार उत्तर सेनाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ—इन सबने हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ते कदम रोक दिए।
- सामन्तीय ढाँचे की अंतर्निहित नाजुकता: जितना विस्तार “सामन्तों” के बल पर हुआ, उसी का राज्य के यथार्थ नियंत्रण पर प्रभाव सीमित रहा। हर्ष के निधन के बाद तेज़ी से साम्राज्य का विखण्डन इसी कारण संभव हुआ।
- राज्य का “व्यक्तिनिष्ठ” (personality-centric) होना: हर्ष की व्यक्तिगत प्रतिभा, कूटनीति, और प्रतिष्ठा ने साम्राज्य को बाँधे रखा; उनके जाते ही कोई उत्तराधिकारी उतना सक्षम/स्थापित नहीं रहा, जिससे एक स्थायी केंद्रीकृत राज-परम्परा बन पाती।
- आर्थिक-सैन्य संसाधनों का संतुलन: इतने विस्तृत क्षेत्र में कर-संग्रह, सैनिक-आपूर्ति, और प्रशासन की एकरूपता बनाए रखना कठिन था। इसलिए हर्ष को धार्मिक-दान, राजसभा, औरकूटनीति के माध्यम से नैतिक-वैधता पर अधिक बल देना पड़ा।
12. निष्कर्ष: हर्ष के साम्राज्य-विस्तार की ऐतिहासिक अर्थवत्ता
हर्ष का साम्राज्य-विस्तार गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में एक बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन का प्रतीक है। उन्होंने:
- कनौज को सत्ता-केंद्र बनाकर गंगा के मैदान को सुदृढ़ राजनीतिक एकता में बाँधा।
- पूर्व (मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा) से लेकर पश्चिम (मालवा, वल्लभी) और उत्तर (कश्मीर, नेपाल) तक व्यापक सामन्त-नेटवर्क तैयार किया।
- दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रोके जाने के बावजूद, नर्मदा तक की सीमा स्थिर की और उत्तर भारत को लगभग चार दशकों तक स्थिर नेतृत्व दिया।
- धर्म-सम्मेलनों, प्रयाग के महादानों, और बौद्ध-संरक्षण के द्वारा अपने साम्राज्य को सांस्कृतिक-वैचारिक वैधता प्रदान की, जिससे सामन्तों और जनमानस में उनकी सर्वोच्चता स्वीकार्य बनी।
- किन्तु उनका साम्राज्य एक “केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य” कम, और “कर-उपहार देने वाले सामन्तों का विस्तृत संघ” अधिक था—इसलिए उनकी मृत्यु के बाद तेजी से क्षेत्रीय राज्यों का पुनरुत्थान हुआ और कनौज स्वयं बहु-राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बन गया (त्रिपक्षीय संघर्ष: प्रतिहार–पाल–राष्ट्रकूट)।
अतः, हर्ष के साम्राज्य-विस्तार का महत्व सिर्फ भू-सीमाओं की दृष्टि से नहीं, बल्कि इस बात से भी है कि उन्होंने गुप्तोत्तर अराजकता के बाद उत्तर भारत को पुनः एक साझा राजनीतिक-धार्मिक मंच दिया, और कनौज को अगले कई शताब्दियों तक भारतीय राजनीति के “ट्रॉफी-शहर” का दर्जा दिलाया। उनके विस्तार की सबसे बड़ी सीमा दक्कन में चालुक्य प्रतिरोध रही, और सबसे बड़ी शक्ति—उत्तरी मैदानों की सैन्य, कूटनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण-क्षमता। यही हर्ष की साम्राज्य-रचना की ऐतिहासिक सच्चाई और विरासत है।