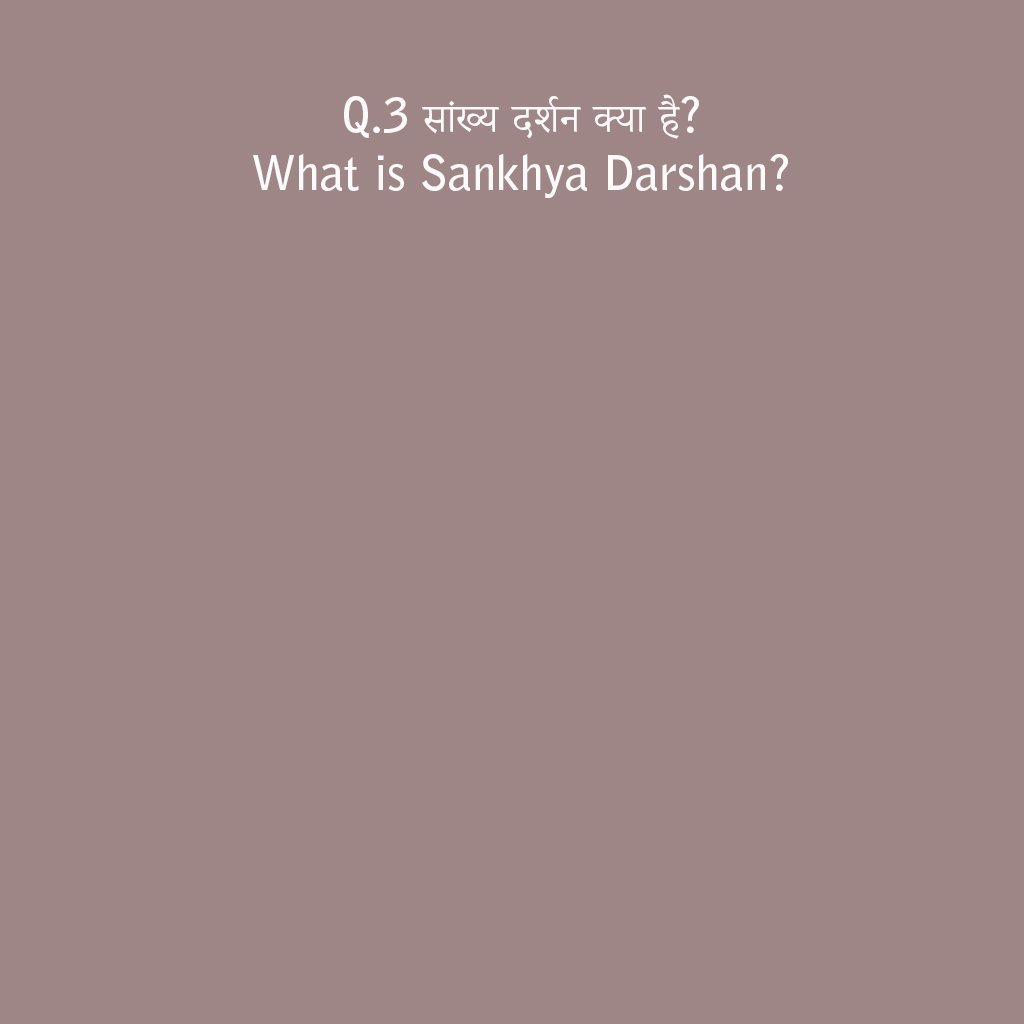सांख्य दर्शन क्या है? What is Sankhya philosophy?
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
परिचय
भारतीय दर्शन परंपरा में कुल छह आस्तिक दर्शनों को मान्यता प्राप्त है – न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त। इन छह दर्शनों में से सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला दर्शन है। “सांख्य” शब्द का अर्थ है “संख्या” या “विचारों का विवेकपूर्ण विश्लेषण”। यह दर्शन तत्वों की गणना और विवेचन पर आधारित है, इसीलिए इसे सांख्य कहा गया।
सांख्य दर्शन का उद्देश्य है – प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझकर मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात् जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाना। यह दर्शन एक नास्तिक दर्शन नहीं है, लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वतः सिद्ध या अनिवार्य नहीं मानता। इसकी प्रमुख विशेषता है – तर्क और अनुभव पर आधारित तत्वों की गणना और विश्लेषण।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक
- आदि प्रवर्तक: कपिल मुनि
- प्रमुख ग्रंथ: सांख्य सूत्र (कपिल), सांख्य कारिका (ईश्वरकृष्ण), तत्त्व कौमुदी (वाचस्पति मिश्र)
सांख्य दर्शन की सबसे प्रसिद्ध रचना है “सांख्य कारिका”, जिसे ईश्वरकृष्ण ने लिखा था। इसमें कुल 72 श्लोकों में पूरे सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया है।
सांख्य दर्शन की विशेषताएँ
- द्वैतवाद – यह दर्शन प्रकृति और पुरुष को दो स्वतंत्र तत्त्व मानता है।
- तत्वमीमांसा (Metaphysics) – इसमें 25 तत्त्वों की व्याख्या की गई है।
- कारणवाद – सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता है, अर्थात् कार्य पहले से ही कारण में निहित होता है।
- ईश्वर का निषेध – यह दर्शन मोक्ष के लिए ईश्वर को अनिवार्य नहीं मानता।
- ज्ञान के माध्यम से मोक्ष – सांख्य दर्शन में मोक्ष केवल ज्ञान (विवेक) से प्राप्त होता है, क्रियाओं (कर्म) से नहीं।
सांख्य दर्शन का उद्देश्य
सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य है –
“दुःखत्रय अभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।”
अर्थात् तीन प्रकार के दुःखों (आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक) से छुटकारा पाने हेतु उनके कारण का ज्ञान और उसका निवारण।
तीन प्रकार के दुःख (त्रिविध दुःख)
- आध्यात्मिक दुःख – मन और शरीर से उत्पन्न, जैसे चिंता, रोग
- आधिभौतिक दुःख – अन्य जीवों या मनुष्यों से उत्पन्न, जैसे हिंसा, शत्रुता
- आधिदैविक दुःख – प्रकृति या दैविक शक्तियों से उत्पन्न, जैसे तूफान, भूकंप
सांख्य दर्शन के दो मुख्य तत्त्व
1. पुरुष (चेतन तत्त्व)
- यह चेतन, अव्यक्त, अक्रिय और निरपेक्ष है।
- यह केवल “द्रष्टा” (द्रष्टा भाव) है, कुछ करता नहीं।
- अनेक पुरुषों की सत्ता को मान्यता प्राप्त है।
2. प्रकृति (अचेतन तत्त्व)
- यह जड़ (अचेतन) है, लेकिन सृजनकारी है।
- इसमें त्रिगुण – सत्व, रज, तम – होते हैं।
- सभी कार्य, सृष्टि, मन, इंद्रियाँ, शरीर आदि प्रकृति से उत्पन्न हैं।
प्रकृति के त्रिगुण (Three Gunas of Prakriti)
| गुण | विशेषताएँ | उदाहरण |
|---|---|---|
| सत्त्व | ज्ञान, प्रकाश, संतुलन | शांतचित्त व्यक्ति, ध्यान |
| रजस् | क्रिया, ऊर्जा, उत्साह | महत्वाकांक्षा, दौड़-भाग |
| तमस् | अज्ञान, जड़ता, निष्क्रियता | आलस्य, नकारात्मकता |
जब ये तीनों गुण संतुलन में होते हैं, तब प्रकृति अव्यक्त रहती है। जब इनमें असंतुलन होता है, तब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
25 तत्त्वों का विवरण (Tattva Vichar)
सांख्य दर्शन में 25 तत्त्व माने गए हैं। ये तत्त्व सृष्टि के निर्माण और आत्मा की मुक्ति के लिए समझे जाते हैं।
| क्रम | तत्त्व | उत्पत्ति |
|---|---|---|
| 1 | प्रकृति | मूल कारण, अव्यक्त |
| 2 | महत्तत्त्व (बुद्धि) | प्रकृति से |
| 3 | अहंकार | महत्तत्त्व से |
| 4–8 | पंच तन्मात्रा – शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध | अहंकार से |
| 9–13 | पंच ज्ञानेन्द्रियाँ – कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक | अहंकार से |
| 14–18 | पंच कर्मेन्द्रियाँ – वाणी, हाथ, पाँव, गुदा, उपस्थ | अहंकार से |
| 19 | मन | अहंकार से |
| 20–24 | पंच महाभूत – आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी | तन्मात्राओं से |
| 25 | पुरुष | स्वतंत्र चेतन |
प्रकृति और पुरुष का संबंध
- प्रकृति सृजन करती है लेकिन जड़ है, चेतना नहीं है।
- पुरुष चेतन है, लेकिन सृजन में भाग नहीं लेता।
- उदाहरण: जैसे नर्तकी (प्रकृति) नाचती है और दर्शक (पुरुष) केवल उसे देखता है।
सांख्य दर्शन कहता है कि जब पुरुष समझ लेता है कि वह प्रकृति से अलग है, तभी उसे मोक्ष मिलता है।
मोक्ष की परिकल्पना (Concept of Liberation)
- मोक्ष का अर्थ है – प्रकृति और पुरुष के बीच का विवेकपूर्ण भेदबोध।
- जब पुरुष यह जान लेता है कि वह सृष्टि, शरीर, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है, तभी वह बंधन से मुक्त होता है।
- मोक्ष की अवस्था में – कोई कर्म नहीं होता, न पुनर्जन्म होता है, न सुख-दुःख।
सांख्य दर्शन में ईश्वर का स्थान
सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि:
- ईश्वर का होना सिद्ध नहीं किया जा सकता।
- यदि ईश्वर है, तो दुःख क्यों है?
- पुरुष और प्रकृति ही सृष्टि के लिए पर्याप्त हैं।
परंतु, सांख्य के बाद योग दर्शन ने ईश्वर को माना और योगसूत्र में उसे “पुरुषोत्तम” के रूप में प्रस्तुत किया।
सांख्य दर्शन और योग दर्शन का संबंध
- योग दर्शन सांख्य दर्शन की क्रियात्मक शाखा है।
- सांख्य “ज्ञान” द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि योग “क्रिया” और “ध्यान” द्वारा।
- दोनों में तत्व मीमांसा समान है – 25 तत्त्व, प्रकृति-पुरुष द्वैतवाद, त्रिगुण सिद्धांत आदि।
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सांख्य दर्शन का महत्व
- मानसिक शांति – आत्मा और शरीर के भेद को जानकर तनाव से मुक्ति।
- स्वतंत्रता का बोध – पुरुष की स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान।
- विज्ञान से साम्य – ऊर्जा, तत्व, चेतना की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से।
- मनोविज्ञान में उपयोगी – मन, बुद्धि, अहंकार की विश्लेषणात्मक समझ।
उदाहरणों द्वारा सांख्य दर्शन की व्याख्या
उदाहरण 1 – टेलीविजन और दर्शक
टीवी पर नाटक चल रहा है, लेकिन दर्शक केवल देखता है, उसमें भाग नहीं लेता। उसी प्रकार पुरुष केवल “द्रष्टा” है, क्रियाओं में लिप्त नहीं है। जो नाटक चल रहा है, वह प्रकृति की रचना है।
उदाहरण 2 – सूर्य और जल का प्रतिबिंब
सूर्य (पुरुष) केवल प्रकाश देता है, लेकिन जल में उसका प्रतिबिंब (प्रकृति) अनेक रंगों और हलचलों के साथ दिखाई देता है। सूर्य शांत रहता है, जल की गति में बदलाव आता है।
सांख्य दर्शन की समालोचना
- सकारात्मक पक्ष:
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण
- तत्त्वों की स्पष्ट गणना
- विवेक पर आधारित मोक्ष
- नकारात्मक पक्ष:
- ईश्वर को नकारने पर आलोचना
- अनुभवात्मक सिद्धांतों की सीमा
- केवल ज्ञान से मोक्ष – साधारण के लिए कठिन
निष्कर्ष
सांख्य दर्शन भारतीय तत्त्वमीमांसा की रीढ़ है। इसने प्रकृति और चेतन पुरुष का ऐसा विवेचन प्रस्तुत किया है जो केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि तात्त्विक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। इसकी विश्लेषणात्मक शैली, तत्त्वों की स्पष्टता, और जीवन के अंतिम उद्देश्य – मोक्ष – को प्राप्त करने की सरल विधि इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।
आज के तनावपूर्ण, भौतिकतावादी युग में यदि मनुष्य इस दर्शन के आधार पर जीवन को समझे, तो उसे अपनी वास्तविक पहचान का बोध होगा और वह शांति, संतुलन और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।