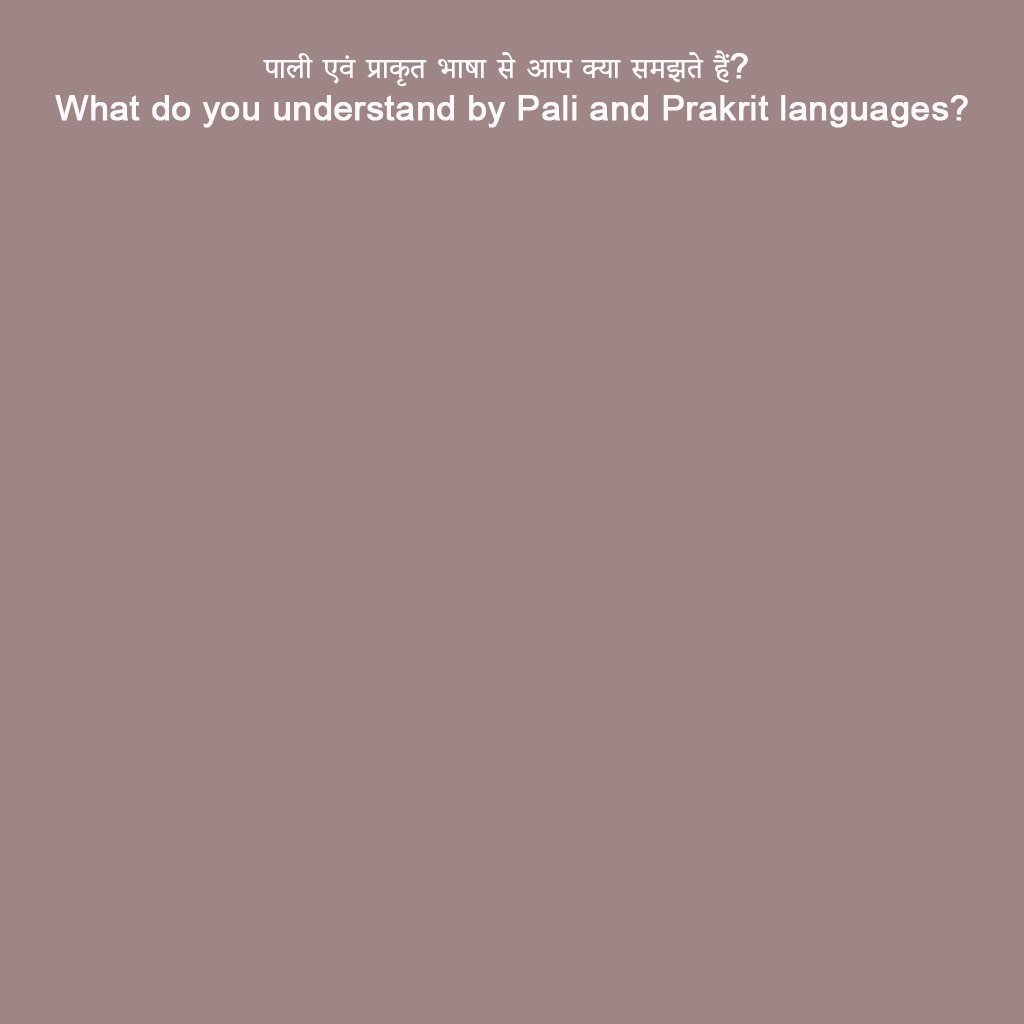पाली एवं प्राकृत भाषा से आप क्या समझते हैं? What do you understand by Pali and Prakrit languages?
शुरुवात से अंत तक जरूर पढ़ें।
परिचय
भारत का भाषाई इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। पाली और प्राकृत भाषाएँ भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन भाषाओं में से हैं, जो विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। ये भाषाएँ उस कालखंड की हैं जब संस्कृत, जो कि एक शुद्ध और क्लिष्ट भाषा मानी जाती थी, आम जनमानस की भाषा नहीं थी। ऐसे में पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं ने जनसामान्य से संवाद का कार्य किया।
पाली और प्राकृत दोनों ही भाषाएँ संस्कृत से निकट संबंध रखती हैं लेकिन ये सरल, बोलचाल की भाषाएँ थीं, जिन्हें सामान्य जनता आसानी से समझ सकती थी। विशेष रूप से इन भाषाओं का उपयोग बौद्ध और जैन साहित्य में प्रमुखता से हुआ।
पाली भाषा: परिचय
पाली भाषा एक मध्य-भारतीय आर्य भाषा है जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के प्रारंभिक साहित्य से संबंधित है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग थेरवादी बौद्ध धर्म के ग्रंथों, विशेष रूप से त्रिपिटक या पालि कैनन में देखने को मिलता है।
पाली शब्द का अर्थ
‘पाली’ शब्द का शाब्दिक अर्थ है “पंक्ति” या “पाठ”। प्रारंभ में पाली शब्द का प्रयोग सिर्फ ग्रंथों के लिए किया जाता था, न कि भाषा के रूप में। लेकिन समय के साथ यह शब्द उस भाषा के लिए भी प्रयुक्त होने लगा जिसमें वे ग्रंथ लिखे गए थे।
पाली भाषा की विशेषताएँ
- सरल व्याकरण: संस्कृत की तुलना में पाली भाषा का व्याकरण सरल है। उदाहरण के लिए, इसमें धातुओं के रूपों में अधिक जटिलता नहीं होती।
- सार्वजनिक संवाद की भाषा: बुद्ध ने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया क्योंकि यह आम जनता की भाषा थी।
- धार्मिक भाषा: पाली को बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा माना जाता है, विशेषकर थेरवादी परंपरा में।
- लेखन शैली: पाली साहित्य में वर्णनात्मक शैली प्रमुख है, जो धार्मिक सिद्धांतों और जीवन मूल्यों को समझाने में सहायक है।
पाली साहित्य
पाली साहित्य मुख्यतः तीन भागों में विभाजित होता है:
1. विनय पिटक (Vinaya Pitaka)
यह ग्रंथ बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संकलन है।
2. सुत्त पिटक (Sutta Pitaka)
इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद संकलित हैं। यह बौद्ध धर्म का मूल धार्मिक ग्रंथ माना जाता है।
3. अभिधम्म पिटक (Abhidhamma Pitaka)
इस भाग में बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान, और तत्त्वमीमांसा का विस्तार से वर्णन मिलता है।
पाली भाषा का महत्व
- पाली भाषा ने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- यह भाषा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के साथ फैली, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि।
- आज भी थेरवादी बौद्ध भिक्षु पाली भाषा का अध्ययन करते हैं और त्रिपिटक का पाठ करते हैं।
प्राकृत भाषा: परिचय
प्राकृत शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है – “प्राकृतिक” या “सामान्य रूप से उत्पन्न”। यह उन भाषाओं को संदर्भित करता है जो संस्कृत से विकसित हुईं और आम जनता द्वारा बोली जाती थीं। प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है बल्कि यह एक भाषाई परिवार है जिसमें कई उपभाषाएँ आती हैं।
प्राकृत भाषा की विशेषताएँ
- सर्वसामान्य भाषा: यह भाषा आम जनता द्वारा बोली जाती थी, इसलिए इसे “लोकभाषा” भी कहा जाता है।
- सरल और प्रवाहपूर्ण: संस्कृत की तुलना में इसमें उच्चारण और शब्द रचना आसान होती है।
- साहित्यिक प्रयोग: अनेक नाटक, कहानियाँ, और धार्मिक ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए हैं।
- भाषिक विविधता: प्राकृत के अनेक रूप थे – जैसे अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री आदि।
प्रमुख प्राकृत भाषाएँ
1. अर्धमागधी
- यह जैन धर्म के ग्रंथों की प्रमुख भाषा थी।
- महावीर स्वामी ने इसी भाषा में उपदेश दिए थे।
- आगम ग्रंथ (जैन धर्मग्रंथ) अर्धमागधी में ही रचे गए।
2. शौरसेनी
- यह पश्चिम भारत की प्रमुख प्राकृत भाषा थी।
- संस्कृत नाटकों में, जैसे कालिदास के नाटकों में, स्त्रियों और विदूषकों के संवाद शौरसेनी प्राकृत में होते थे।
3. महाराष्ट्री
- यह दक्षिण-पश्चिम भारत में बोली जाती थी।
- यह प्राकृत काव्य की भाषा थी, जैसे कि गाथा सप्तशती इसी भाषा में लिखी गई।
4. पैशाची प्राकृत
- यह एक लुप्तप्राय प्राकृत भाषा है, जिसे ‘राक्षसी भाषा’ भी कहा जाता था।
- प्रसिद्ध कथा ग्रंथ बृहत्कथा इसी में लिखा गया था।
प्राकृत साहित्य
प्राकृत में विशाल साहित्य की रचना हुई जिसमें धार्मिक, काव्य, नाट्य और लोककथाएँ शामिल हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण:
- गाथा सप्तशती (गाथाओं का संग्रह)
- जैन आगम (जैन धर्मग्रंथ)
- प्राकृत नाटक (शूद्रक का मृच्छकटिकम् आदि)
- बृहत्कथा (कथाओं का विशाल संग्रह)
पाली और प्राकृत का तुलनात्मक अध्ययन
| विशेषता | पाली | प्राकृत |
|---|---|---|
| भाषा का प्रयोग | बौद्ध धर्म में | जैन धर्म, साहित्य, नाटकों में |
| साहित्यिक शैली | धार्मिक उपदेशात्मक | धार्मिक + काव्यात्मक + नाटकीय |
| विकास काल | लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व | लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठीं सदी ई. तक |
| व्याकरण | सरल | बहुत विविध |
| क्षेत्र | भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आदि | भारत के विभिन्न भाग |
| उपभाषाएँ | एकरूप भाषा | कई उपभाषाएँ (अर्धमागधी, शौरसेनी आदि) |
पाली और प्राकृत की वर्तमान स्थिति
आज ये भाषाएँ जनभाषाएँ नहीं रहीं, लेकिन शास्त्रीय और शैक्षणिक दृष्टिकोण से इनका महत्व बरकरार है। विश्वविद्यालयों में इनका अध्ययन होता है, और बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबियों के बीच इनका पठन-पाठन अभी भी जारी है।
पाली और प्राकृत का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव
- धार्मिक विचारों का प्रचार: इन भाषाओं ने जटिल धार्मिक विचारों को सरल भाषा में जनता तक पहुँचाया।
- साहित्यिक परंपरा का विकास: नाट्य, काव्य और गद्य साहित्य की नींव प्राकृत भाषाओं में रखी गई।
- लोकसंस्कृति की अभिव्यक्ति: इन भाषाओं में आम जनता की सोच, भावनाएँ और कहानियाँ प्रतिबिंबित होती हैं।
निष्कर्ष
पाली और प्राकृत भाषाएँ भारतीय भाषाई परंपरा की आत्मा रही हैं। इन्होंने संस्कृत जैसी शास्त्रीय और कठिन भाषा को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने का कार्य किया। चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, इन दोनों ही परंपराओं ने पाली और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग कर धर्म को लोकजीवन से जोड़ा। साथ ही, साहित्यिक क्षेत्र में भी इन भाषाओं ने अनमोल योगदान दिया।
आज भी इन भाषाओं के अध्ययन से हमें न केवल भारत की प्राचीन संस्कृति, धर्म और समाज की गहरी समझ मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी सशक्त साधन हो सकती है।